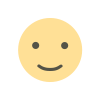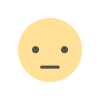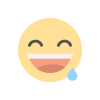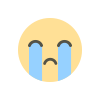प्रधानमंत्री के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और आक्रामक नारे भी लगाए गए ,किसके नारे पर मीडिया चुप रहा और किसके नारे पर पूरा देश खड़ा कर दिया गया ?
UGC के नए नियमों के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान लगाए गए आपत्तिजनक नारों पर मुख्यधारा मीडिया की चुप्पी ने एक बार फिर दोहरे मापदंडों की बहस को जन्म दिया है। सवाल यह है कि जब ऐसे ही नारे JNU या हाशिए के समुदायों से जुड़े कैंपसों में लगते हैं, तो उन्हें देशविरोधी क्यों कहा जाता है, जबकि जनरल वर्ग के प्रदर्शनों पर मीडिया खामोश रहता है। यह रिपोर्ट भारतीय मीडिया की सामाजिक संरचना, जातिगत सोच और चयनात्मक राष्ट्रवाद की गहराई से पड़ताल करती है।

UGC विरोध, दोहरे पैमाने और मीडिया की चुप्पी: सवाल नारे का नहीं, नज़रिये का है
देश में जब भी विश्वविद्यालयों और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर आंदोलन होते हैं, एक सवाल बार-बार उभरकर सामने आता है—क्या हर विरोध को एक ही तराजू में तौला जाता है? या फिर विरोध करने वाले की जाति, पहचान और सामाजिक पृष्ठभूमि तय करती है कि वह “लोकतांत्रिक असहमति” कहलाएगा या “देशद्रोह”?
हाल ही में UGC के नए नियमों के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्रों और युवाओं के प्रदर्शन ने इसी सवाल को फिर से ज़िंदा कर दिया है। इस बार खास बात यह रही कि प्रदर्शन में बड़ी संख्या में जनरल कैटेगरी से जुड़े लोग भी शामिल थे, और कई जगहों पर सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और आक्रामक नारे भी लगाए गए।

विडंबना यह है कि इन नारों पर न तो प्राइम-टाइम डिबेट हुई, न स्टूडियो में चीख-पुकार, और न ही “देश की सुरक्षा” का खतरा बताया गया।
यही वह बिंदु है, जहाँ से असली बहस शुरू होती है।
जब नारा JNU में लगता है, तब देश खतरे में क्यों आ जाता है?
पिछले एक दशक का मीडिया रिकॉर्ड उठाकर देखिए।
जब भी JNU, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जामिया या किसी ऐसे कैंपस में—जहाँ बड़ी संख्या में SC, ST, OBC या अल्पसंख्यक छात्र पढ़ते हैं—सरकार के खिलाफ नारे लगते हैं, तो पूरा मीडिया तंत्र जैसे एक साथ सक्रिय हो जाता है।
शब्द तय होते हैं:
“टुकड़े-टुकड़े गैंग”
“अर्बन नक्सल”
“देशविरोधी मानसिकता”
“देश के दुश्मन”

एंकर सवाल नहीं पूछते, फैसला सुनाते हैं।
स्टूडियो में बैठे पैनलिस्ट पहले से तय कर लेते हैं कि कौन दोषी है और कौन राष्ट्रभक्त।
लेकिन सवाल यह है कि
UGC विरोध के दौरान खुलेआम सरकार विरोधी और हिंसक भाव वाले नारे लगने के बावजूद मीडिया क्यों खामोश रहा?
क्या नारे की भाषा बदली थी? नहीं।
तो फिर नज़र क्यों बदली?**
यह कहना तथ्यात्मक रूप से गलत होगा कि इस बार नारे “सॉफ्ट” थे।
कई वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जिनमें सीधे-सीधे सत्ता के खिलाफ उग्र शब्दों का प्रयोग हुआ।
लेकिन फर्क यह था कि—
प्रदर्शन करने वाले मुख्यधारा सामाजिक वर्ग से थे
आंदोलन को “कानून-व्यवस्था की चुनौती” नहीं बताया गया
पुलिस कार्रवाई पर सवाल नहीं उठे
किसी पर NSA, UAPA या राजद्रोह की चर्चा तक नहीं हुई
यह चयनात्मक चुप्पी अपने-आप में एक बयान है।
मीडिया की संरचना - सवाल विचारधारा का नहीं, सामाजिक ढांचे का है
भारत का मुख्यधारा मीडिया किसके हाथ में है—यह कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं है।
न्यूज़रूम से लेकर बोर्डरूम तक,
निर्णय लेने वाली जगहों पर एक खास सामाजिक वर्ग का वर्चस्व दशकों से बना हुआ है।
यह आरोप नहीं, बल्कि कई स्वतंत्र अध्ययनों और रिपोर्ट्स से सामने आई सच्चाई है कि:
संपादक
एंकर
ओपिनियन-शेपर
इनमें हाशिए के समुदायों की भागीदारी नगण्य है।
जब न्यूज़रूम एक-जैसे सामाजिक अनुभवों से बना होगा, तो
खबरों की संवेदना भी उसी दायरे में कैद रहेगी।
यही कारण है कि—
“अपने जैसे लोगों” के गुस्से को भावनात्मक प्रतिक्रिया माना जाता है
और “दूसरों” के गुस्से को राष्ट्र के लिए खतरा
जाति यहाँ गाली नहीं, संरचना है
अक्सर इस बहस को खारिज करने के लिए कहा जाता है—
“हर बात में जाति क्यों घसीटते हो?”
लेकिन सच्चाई यह है कि
जाति भारत में केवल पहचान नहीं, शक्ति की संरचना है।
यह तय करती है:
कौन बोलेगा
कौन सुना जाएगा
कौन सवाल पूछेगा
और कौन जेल जाएगा
अगर यही नारे JNU में लगते—
तो अब तक:
FIR दर्ज हो चुकी होती
सोशल मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता
परिवारों की पृष्ठभूमि खंगाली जाती
विदेशी फंडिंग और साजिश के एंगल जोड़े जाते
लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ।
कानून सबके लिए समान है—काग़ज़ों में

संविधान कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है।
लेकिन व्यवहार में कानून का प्रयोग समान नहीं, चयनात्मक है।
पिछले वर्षों में हमने देखा है:
-
छात्रों पर UAPA
-
सामाजिक कार्यकर्ताओं पर लंबी हिरासत
-
लेखकों, प्रोफेसरों पर राजद्रोह
और दूसरी ओर,
-
खुलेआम नफरत फैलाने वाले बयान
-
हिंसा भड़काने वाले भाषण
-
लोकतांत्रिक संस्थाओं को गाली
इन पर या तो कार्रवाई नहीं होती, या बेहद हल्की होती है।
UGC विरोध के मामले में भी यही पैटर्न दिखा।
यह चुप्पी भी एक पक्ष है
मीडिया अक्सर दावा करता है कि वह “न्यूट्रल” है।
लेकिन पत्रकारिता में न्यूट्रल होना नहीं, निष्पक्ष होना ज़रूरी है।
जब एक ही तरह की घटना पर—
-
अलग-अलग पैमाने
-
अलग भाषा
-
अलग प्रतिक्रिया
दिखे, तो वह निष्पक्षता नहीं, सांस्थानिक पक्षपात कहलाता है।
UGC विरोध पर मीडिया की चुप्पी दरअसल यह दिखाती है कि
कौन सवाल पूछने के लायक माना जाता है और कौन नहीं।
देश की असली हक़ीक़त यही है
यह देश की हक़ीक़त है कि—
-
लोकतंत्र केवल वोट तक सीमित होता जा रहा है
-
असहमति की परिभाषा जाति और पहचान से तय हो रही है
-
मीडिया सत्ता का नहीं, सामाजिक वर्चस्व का विस्तार बनता जा रहा है
यह रिपोर्ट किसी एक नारे का समर्थन या विरोध नहीं करती।
यह उस दोहरे मापदंड पर सवाल उठाती है,
जो लोकतंत्र को भीतर से खोखला करता है।
सवाल नारा नहीं, नज़र है
आज सवाल यह नहीं है कि
किसने क्या नारा लगाया।
सवाल यह है कि—
-
किसके नारे पर मीडिया चुप रहा
-
और किसके नारे पर पूरा देश खड़ा कर दिया गया
जब तक इस फर्क को समझा नहीं जाएगा,
तब तक “राष्ट्रवाद” केवल एक हथियार रहेगा,
और “लोकतंत्र” सिर्फ़ एक शब्द।
देश को नारे से नहीं, न्याय से जोड़ा जाता है।

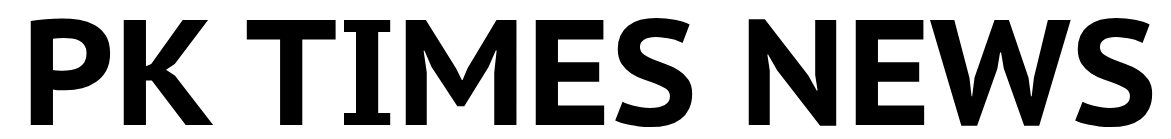
 Hindu Solanki
Hindu Solanki